भारतीय दंड संहिता
आईपीसी धारा 59- (निरस्त) कारावास के बजाय निर्वासन
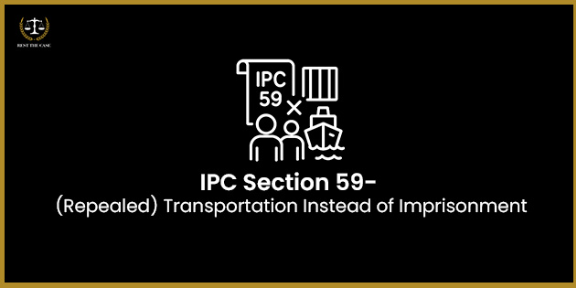
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, भारतीय दंड व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रयोग किया जाता था, जिनमें से सबसे कठोर दंड था परिवहन, जो निर्वासन का एक रूप था, जिसमें दोषियों को अंडमान द्वीप समूह जैसे दंडात्मक उपनिवेशों में भेज दिया जाता था। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 59 में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन का प्रावधान किया गया है: आजीवन कारावास के बजाय निर्वासन का कानूनी विकल्प। हालांकि इस प्रावधान को दशकों पहले निरस्त कर दिया गया था, लेकिन यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि ब्रिटिश भारत सजा को कैसे देखता था और स्वतंत्रता के बाद दंडात्मक प्रथाओं में क्या बदलाव आया।
इस ब्लॉग में हम क्या जानेंगे:
- आईपीसी धारा 59 का मूल अर्थ और कानूनी व्याख्या
- ब्रिटिश भारत में निर्वासन की अवधारणा और व्यवहार
- आजीवन कारावास के विकल्प के रूप में निर्वासन की पेशकश क्यों की गई थी
- इस प्रावधान का निरस्तीकरण और इसकी आधुनिक समय की अप्रासंगिकता
- 1955 के बाद इस तरह की सजा की जगह किसने ली
- ऐतिहासिक कानूनी विश्लेषण के लिए धारा 59 का अभी भी महत्व क्यों है
आईपीसी धारा क्या थी 59?
कानूनी पाठ (निरसन से पहले):
"प्रत्येक मामले में जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास से दंडनीय है, सजा आजीवन निर्वासन हो सकती है।"
सरलीकृत स्पष्टीकरण:
धारा 59 ने अदालतों को आजीवन कारावास के स्थान पर आजीवन निर्वासन देने की अनुमति दी। हालांकि दोनों का उद्देश्य कठोर दंड देना था, लेकिन निर्वासन का एक अनूठा औपनिवेशिक चरित्र था - यह अपराधी को भारतीय मुख्य भूमि से शारीरिक रूप से दूर कर देता था, अक्सर दूर स्थित दंडात्मक कालोनियों में, जिससे सामाजिक और भौगोलिक अलगाव दोनों पैदा होते थे।
इस प्रावधान ने न्यायपालिका को भारतीय जेलों में कारावास के बजाय निर्वासन लागू करने का विवेकाधीन अधिकार प्रदान किया।
परिवहन के अभ्यास को समझना
औपनिवेशिक भारत में, निर्वासन में दोषियों को, विशेष रूप से हत्या, डकैती या राजनीतिक विद्रोह जैसे गंभीर अपराधों में शामिल दोषियों को अंडमान द्वीप समूह में सेलुलर जेल जैसी दंडात्मक कालोनियों में भेजना शामिल था। ये उपनिवेश निम्न के लिए जाने जाते थे:
- कठोर जीवन स्थितियां
- जबरन कठोर श्रम
- समाज से पूर्ण अलगाव
परिवहन केवल एक सजा नहीं थी; यह शाही नियंत्रण का एक उपकरण था, जिसका उपयोग विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों (जैसे, वीर सावरकर) जैसे राजनीतिक कैदियों के लिए किया जाता था। इसने दंड को निर्वासन के साथ जोड़ दिया, जिससे असहमति रखने वालों को भारतीय समाज से प्रभावी रूप से हटा दिया गया।
धारा 59 का उद्देश्य और अनुप्रयोग
धारा 59 ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की:
- सजा में लचीलापन: न्यायाधीशों को उपयुक्त मामलों में आजीवन कारावास की बजाय निर्वासन का विकल्प चुनने की अनुमति दी।
- राजनीतिक सुविधा: ब्रिटिश सरकार को उन व्यक्तियों को हटाने में मदद की जो औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए खतरा थे।
- : निर्वासन के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आघात के माध्यम से बढ़ी हुई रोकथाम।
- एक समान अनुप्रयोग: ब्रिटिश भारत में विभिन्न न्यायालयों में गंभीर अपराधों के लिए दंड देने के तरीके को मानकीकृत किया गया।
स्वतंत्रता के बाद निरसन और अतिरेक
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, औपनिवेशिक युग की दंड प्रथाओं से दूर जाने का एक सचेत प्रयास किया गया। परिवहन का विचार, अपनी अंतर्निहित क्रूरता और मानव अधिकारों से अलगाव के कारण, भारतीय संविधान के साथ असंगत था।
निरसन के कारण:
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: परिवहन अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के साथ संघर्ष करता था।
- अमानवीय स्थितियाँ: सज़ा अत्यधिक कठोर थी और इसमें पुनर्वास की कमी थी इरादा।
- अतिरेक: एक संरचित जेल प्रणाली के साथ, परिवहन अप्रचलित हो गया।
- विधायी सुधार: दंड प्रक्रिया संहिता और जेल अधिनियम उचित प्रक्रिया और कैदी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विकसित हुए।
परिणामस्वरूप, आईपीसी धारा 59 को 1955 में 1955 के अधिनियम 10 द्वारा औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया, जिसने आईपीसी में परिवहन के सभी संदर्भों को भी हटा दिया।
धारा 59 का स्थान किसने लिया 59?
निरसन के बाद, निर्वासन के स्थान पर आजीवन कारावास ही अधिकतम सज़ा बना रहा। आज:
- आईपीसी की धारा 53 आजीवन कारावास को सज़ा के एक मान्यता प्राप्त रूप के रूप में रेखांकित करती है।
- गंभीर अपराधों में कठोर कारावास (कठोर श्रम के साथ) लगाया जाता है।
- सीआरपीसी और कारागार अधिनियम यह परिभाषित करते हैं कि दोषियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसमें गरिमा और पुनर्वास पर ज़ोर दिया गया है।
यह अभी भी क्यों मायने रखता है
हालाँकि अब यह धारा लागू नहीं है, फिर भी आईपीसी की धारा 59 भारत के कानूनी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि:
- यह उस औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है जो सज़ा को सुधार के बजाय निर्वासन मानती थी।
- यह समझने में मदद करता है कि कैसे भारतीय न्याय व्यवस्था शाही मूल्यों से संवैधानिक मूल्यों की ओर परिवर्तित हुई।
- कानूनी इतिहास, आपराधिक न्यायशास्त्र और न्यायिक प्रशिक्षण में इसका बार-बार उल्लेख किया जाता है।
- यह स्वतंत्रता के बाद के युग में मानवीय दंड मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
निष्कर्ष
आईपीसी की धारा 59 ने कभी औपनिवेशिक अदालतों को आजीवन कारावास के बजाय निर्वासन की शक्ति दी थी। इसका अस्तित्व उस युग को दर्शाता है जहाँ सज़ा सुधार में नहीं, बल्कि प्रतिशोध और निर्वासन में निहित थी। इसके निरसन ने भारत के सम्मान, समानता और संवैधानिक नैतिकता पर आधारित न्याय प्रणाली की ओर बदलाव को चिह्नित किया। धारा 59 जैसे निरस्त प्रावधानों का अध्ययन करके, कानूनी विद्वानों और छात्रों को इस बात की गहरी समझ प्राप्त होती है कि भारत ने अपने दंड कानूनों को मानवीय बनाने में कितनी प्रगति की है - और हमारी न्याय प्रणाली पर औपनिवेशिक विरासत का स्थायी प्रभाव क्या है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1. आईपीसी की धारा 59 क्या थी?
इसने अदालतों को गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास के स्थान पर आजीवन निर्वासन की सजा देने की अनुमति दे दी।
प्रश्न 2. दण्ड के रूप में निर्वासन से क्या तात्पर्य है?
परिवहन में दोषियों को अंडमान द्वीप समूह जैसे दूरस्थ दंडात्मक उपनिवेशों में निर्वासित करना शामिल था, जिसमें कारावास, कठोर श्रम और एकांतवास शामिल था।
प्रश्न 3. क्या धारा 59 अभी भी लागू है?
नहीं, आईपीसी की धारा 59 को 1955 में निरस्त कर दिया गया था जब भारत में दंड के रूप में निर्वासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी।
प्रश्न 4. भारतीय कानून में परिवहन का स्थान किसने ले लिया?
अब गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास और कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता और जेल नियम अब सज़ा सुनाए जाने के बाद की हिरासत को नियंत्रित करते हैं।
प्रश्न 5. यह खंड अभी भी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
यह भारत के दंड इतिहास पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, औपनिवेशिक कानूनी ढांचे का विश्लेषण करने में मदद करता है, और भारतीय आपराधिक कानून में मानवाधिकारों के विकास पर प्रकाश डालता है।






