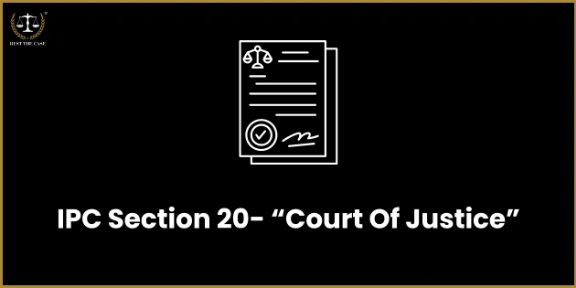
6.1. 1. क्वीन एम्प्रेस बनाम तुलजा (1887)
6.2. 2. ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण
6.3. 3. श्री बलवान सिंह बनाम श्री लक्ष्मी नारायण और अन्य
7. निष्कर्ष 8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)8.1. प्रश्न 1. आईपीसी धारा 19 के अंतर्गत "न्यायालय" का क्या अर्थ है?
8.2. प्रश्न 2. क्या इसमें सरकार का हर अधिकारी शामिल है?
8.3. प्रश्न 3. "न्यायाधीश" और "न्यायालय" के बीच क्या अंतर है?
आपराधिक कानून में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कानूनी कार्यवाही करने और निर्णय सुनाने का अधिकार किसके पास है। यहीं पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत “न्यायालय” की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। आईपीसी की धारा 19 इस शब्द को परिभाषित करती है, जो झूठी गवाही, न्याय में बाधा डालने या न्यायिक अधिकारियों पर हमला करने जैसे विभिन्न अपराधों की व्याख्या करने की नींव रखती है।
यह ब्लॉग आपको यह समझने में मदद करेगा:
- आईपीसी के तहत "न्यायालय" की कानूनी परिभाषा
- इस परिभाषा के अंतर्गत न्यायालय कौन है?
- वास्तविक जीवन निहितार्थ और कानूनी प्रासंगिकता
- इसके अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण
- प्रासंगिक मामले कानून और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
“न्यायालय” की कानूनी परिभाषा – आईपीसी धारा 19
नंगे अधिनियम पाठ :
"न्यायालय" शब्द ऐसे न्यायाधीश को सूचित करते हैं, जिसे विधि द्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, या न्यायाधीशों के एक निकाय को सूचित करते हैं, जिसे विधि द्वारा एक निकाय के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा हो। उदाहरण मद्रास संहिता के 22 विनियमन VII, 1816 के अंतर्गत कार्य करने वाली पंचायत, जिसके पास मुकदमों की सुनवाई करने और निर्धारण करने की शक्ति है, न्यायालय है।"
सरलीकृत स्पष्टीकरण:
एक तरफ, न्यायालय कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होगा जिसके पास न्यायिक निर्णय देने की कानूनी शक्ति होगी, बशर्ते कि वे न्यायिक क्षमता में काम कर रहे हों। यही परिभाषा कुछ आपराधिक अपराधों की प्रयोज्यता को विशेष रूप से झूठे साक्ष्य देने, अवमानना या न्यायिक कार्यवाही के दौरान किए गए किसी भी अपराध से संबंधित मामलों में निर्धारित करती है।
आईपीसी के तहत "न्यायालय" के रूप में कौन योग्य है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अनुसार, "न्यायालय" का अर्थ है:
- एक व्यक्तिगत न्यायाधीश
उदाहरण के लिए, किसी आपराधिक मुकदमे में न्यायिक रूप से कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कहलाता है।
- न्यायाधीशों की एक पीठ या पैनल
ऐसे अवसर पर जब न्यायाधीशों का एक समूह, जैसे कि उच्च न्यायालय का एक समूह, किसी मामले की सुनवाई करता है और निर्णय देता है, तो ये न्यायाधीश एक साथ मिलकर न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे।
- केवल न्यायिक रूप से कार्य करते समय
यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यायाधीश या न्यायाधीशों को न्यायिक कार्य करना चाहिए, अर्थात किसी मामले की सुनवाई करना, साक्ष्य पर विचार करना, निर्णय लेना या कानून लागू करना। प्रशासनिक या गैर-न्यायिक क्षमता में कार्य करते समय वे न्यायालय नहीं कहलाते।
आईपीसी धारा 19 का व्यावहारिक महत्व
"न्यायालय" के रूप में कार्य करने वाले न्यायाधीशों या न्यायिक निकायों की परिभाषा इस प्रकार है:
- आईपीसी की अन्य धाराओं का अनुप्रयोग
कुछ धाराएं आईपीसी के प्रावधानों के समान हैं, जैसे:
- धारा 193- न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देना।
- धारा 228 - न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक का जानबूझकर अपमान करना; अर्थात्, जब इन धाराओं को लागू किया जाना हो, तो आईपीसी धारा 19 के तहत परिभाषित न्यायालय का सहारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल तभी जब कार्य न्यायालय के समक्ष किया जाता है, तो यह अपराध बन जाता है।
- न्यायिक पदाधिकारी को संरक्षण और निहित प्रतिरक्षा
संक्षेप में, आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आदि द्वारा निर्धारित प्रचुर प्रतिरक्षा अक्सर उन लोगों को प्रदान की जाती है जो "न्यायालय" के रूप में कार्य करते हैं। इस संदर्भ में की गई कार्रवाई को तब तक प्रतिरक्षा प्राप्त होती है जब तक यह साबित न हो जाए कि यह दुर्भावनापूर्ण या अधिकार क्षेत्र से बाहर की गई है।
आईपीसी धारा 19 को दर्शाने वाले उदाहरण
उदाहरण 1:
सिविल जज भूमि मामले में विवाद की सुनवाई करता है, गवाह का बयान दर्ज करता है और फैसला सुनाता है। इन सभी कार्यों में न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है। किसी भी गवाह ने गलत बयान दिया हो सकता है, जिसके लिए न्यायालय के समक्ष गलत साक्ष्य देने के लिए धारा 193 आईपीसी के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं।
उदाहरण 2:
चोरी के मामले में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गैर-जमानती वारंट जारी करता है। यदि उसे रिश्वत देने या अपमानित करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो यह झूठी गवाही के अर्थ में "न्यायालय" के विरुद्ध अपराध माना जाएगा।
उदाहरण 3:
यदि वही न्यायाधीश बाद में कर्मचारियों को निर्देश देते हुए पाया जाता है कि अदालती फाइलों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो यह प्रशासनिक कार्य "न्यायालय" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
"न्यायालय" को परिभाषित करने का कानूनी महत्व
"न्यायालय" की परिभाषा निम्नलिखित में सहायता करती है:
- क्षेत्राधिकार का निर्धारण: यह सुनिश्चित करना कि मामला केवल उन न्यायिक प्राधिकारियों के पास भेजा जाए जिनके पास ऐसा करने का क्षेत्राधिकार है।
- आरोप तय करना: झूठी गवाही के मामलों को स्पष्ट करने के लिए, उदाहरण के लिए, कि क्या झूठ न्यायिक परिवेश में बोला गया था।
- न्यायालय की गरिमा बनाए रखना: कानून न्यायिक प्रक्रियाओं की गरिमा को स्वीकार करता है और ऐसी गरिमा की रक्षा करता है।
- दुरुपयोग पर अंकुश लगाना: यह इन संरक्षणों के अनुप्रयोग को प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं करता, बल्कि न्यायिक कार्यों तक सीमित कर देता है।
'न्यायालय' पर ऐतिहासिक मामला
आईपीसी धारा 19 के तहत "न्यायालय" के दायरे और व्याख्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए, यहां कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं जो स्पष्ट करते हैं कि भारतीय अदालतों ने वास्तविक दुनिया के कानूनी संदर्भों में इस प्रावधान को कैसे परिभाषित और लागू किया है।
1. क्वीन एम्प्रेस बनाम तुलजा (1887)
न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय
मुद्दा: यह तय करना कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा न्यायिक चरित्र में किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अंतर्गत "न्यायालय" के समान है।
निर्णय: क्वीन एम्प्रेस बनाम तुलजा (1887) में न्यायालय ने माना कि किसी इकाई को "न्यायालय" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यायिक कार्य संभालने के लिए कानून द्वारा सशक्त होना चाहिए। प्रशासनिक कार्य या अन्य जो गैर-न्यायिक हैं, उनके मात्र निष्पादन में, पर्याप्त नहीं हो सकते।
2. ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
मुद्दा: क्या जांच आयोग को भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अंतर्गत वर्णित "न्यायालय" के अर्थ में शामिल किया जा सकता है।
ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जांच आयोग को "न्यायालय" के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके पास बाध्यकारी निर्णय देने की शक्ति नहीं है।
3. श्री बलवान सिंह बनाम श्री लक्ष्मी नारायण और अन्य
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
मुद्दा: चुनाव याचिकाओं के विषय पर न्यायिक प्राधिकार और उसकी रूपरेखा की व्याख्या।
श्री बलवान सिंह बनाम श्री लक्ष्मी नारायण एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाओं में विवरण की आवश्यकता और ऐसे मामलों से निपटने वाले न्यायिक निकायों के लिए निहितार्थ पर चर्चा की।
निष्कर्ष
इसके अलावा, आईपीसी धारा 19 के ढांचे के भीतर ही वह आधार पाया जा सकता है जिस पर भारत में न्यायालय की परिभाषा टिकी हुई है। यह परिभाषा आगे चलकर अन्य गंभीर अपराधों, जैसे कि झूठे साक्ष्य देना या न्यायाधीश का अपमान करना या अवमानना करना, के लिए अभियोजन के तरीके को नियंत्रित करती है। यह रेखा इतनी बारीक होगी कि केवल वैध प्राधिकरण के तहत न्यायिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही न्यायालय के रूप में मान्यता दी जाएगी।
किसी भी कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए इस खंड पर पकड़ होना ज़रूरी है-चाहे वह मुक़दमाकर्ता, गवाह, प्रॉक्सी, वकील या कोई अन्य लोक सेवक हो। इस तरह, यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायपालिका में सभी भूमिकाओं का सम्मान, संरक्षण और परिभाषा हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या आपके पास अभी भी IPC धारा 19 के बारे में प्रश्न हैं? यहाँ कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं जो “न्यायालय” की परिभाषा से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं, व्यावहारिक निहितार्थों और सामान्य शंकाओं को स्पष्ट करने में मदद करेंगे।
प्रश्न 1. आईपीसी धारा 19 के अंतर्गत "न्यायालय" का क्या अर्थ है?
वे न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समूह जिन्हें न्यायिक रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, जैसे साक्ष्य सुनना, निर्णय पारित करना और विवादों का समाधान करना।
प्रश्न 2. क्या इसमें सरकार का हर अधिकारी शामिल है?
नहीं। केवल वे लोग ही इसमें शामिल हैं जो न्यायिक रूप से कार्य करते हैं और जिन्हें कानूनी रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। अन्य प्रशासनिक अधिकारी या अर्ध-न्यायिक अधिकारी जो न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करते हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।
प्रश्न 3. "न्यायाधीश" और "न्यायालय" के बीच क्या अंतर है?
न्यायाधीश न्यायिक शक्तियों से संपन्न व्यक्ति होता है (आईपीसी धारा 20 में परिभाषित)। न्यायालय न्यायिक रूप से कार्य करने वाला न्यायाधीश (या न्यायाधीश) होता है, जिसे सामूहिक रूप से परीक्षण या कार्यवाही करने वाले कानूनी निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।
प्रश्न 4. क्या न्यायाधिकरण को न्यायालय माना जाता है?
केवल तभी जब न्यायाधिकरण या उसके सदस्य न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए कानून के तहत अधिकृत हों और उनकी कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की हो (जैसे, विवादों का निपटारा करना, लागू करने योग्य निर्णय देना)।





