भारतीय दंड संहिता
आईपीसी धारा 57- दंड की शर्तों के अंश
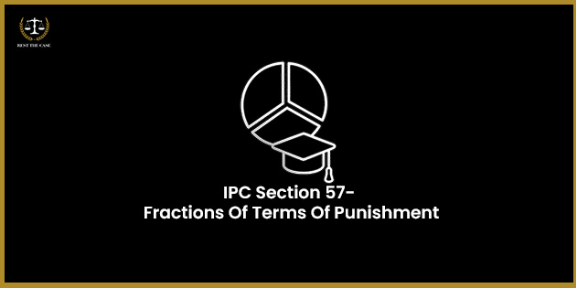
आपराधिक कानून में, सटीकता बेहद ज़रूरी है, खासकर जब सज़ा की अवधि की गणना की बात आती है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ऐसा ही एक प्रावधान धारा 57 है, जो लंबी अवधि की सज़ाओं के अंशों की व्याख्या करने के तरीके से संबंधित है, खासकर आजीवन कारावास के मामलों में। हालांकि यह एक तकनीकी नियम लग सकता है, लेकिन आईपीसी की धारा 57 सज़ा की गणना, छूट, पैरोल की पात्रता और यह आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि क्या कोई अपराधी विशेष कानूनों के तहत रियायत के योग्य है। यह सजा को कम या परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन प्रशासनिक या वैधानिक उद्देश्यों के लिए अनिश्चित दंड को मापने का एक कानूनी तरीका प्रदान करता है।
इस ब्लॉग में हम क्या खोजेंगे:
- आईपीसी धारा 57 की कानूनी परिभाषा और सरलीकृत अर्थ
- दंड की आंशिक गणना क्यों आवश्यक है
- धारा 57 आजीवन कारावास और संबंधित सजाओं पर कैसे लागू होती है
- पैरोल, छूट और पात्रता जांच में धारा 57 का उपयोग
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत आईपीसी 57 की स्थिति
- न्यायिक व्याख्या और उदाहरण
आईपीसी की धारा 57 क्या है?
कानूनी पाठ:
"दंड की अवधि के अंशों की गणना करते समय, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा।"
सरलीकृत व्याख्या:
धारा 57 का अर्थ यह नहीं है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष तक सीमित है। इसमें केवल यह प्रावधान है कि सजा के अंशों, जैसे एक-तिहाई या आधे, की गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि पैरोल नियम के तहत सज़ा का एक-तिहाई हिस्सा पूरा करना ज़रूरी है, तो 20 साल का एक-तिहाई (यानी, 6 साल और 8 महीने) आजीवन कारावास की सज़ा काटने वाले अपराधी के लिए सीमा मानी जा सकती है।
आंशिक गणना क्यों मायने रखती है?
कई आपराधिक कानून और जेल नियम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं:
- आधी सज़ा काटने के बाद
- 14 साल बाद छूट के लिए पात्र
- अगर सज़ा 7 साल से ज़्यादा हो, तो अयोग्य
ऐसे नियमों को लागू करने के लिए, अदालतों और जेल अधिकारियों को आजीवन कारावास को दर्शाने के लिए एक निश्चित संख्या की ज़रूरत होती है। आईपीसी की धारा 57 प्रशासनिक गणना के लिए 20 साल का मानक मान देकर इस समस्या का समाधान करती है।
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण:
यह धारा आजीवन कारावास की सज़ा नहीं देती। कानूनी तौर पर, आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, जब तक कि सरकार द्वारा या संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से सजा को कम या माफ नहीं किया जाता है।
न्यायिक व्याख्या
भारतीय अदालतों ने कई मामलों में धारा 57 के सीमित दायरे की व्याख्या की है।
- गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1961 एससी 600):
गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1961 एससी 600) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी का पूरा जीवनकाल। धारा 57 का उपयोग केवल तब किया जाता है जब कानून या नियमों में सजा के एक अंश की गणना करने की आवश्यकता होती है। - अशोक कुमार @ गोलू बनाम भारत संघ (2021):
अशोक कुमार @ गोलू बनाम भारत संघ (2021), के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 57 आजीवन कारावास की प्रकृति को नहीं बदलती है, लेकिन पैरोल या छूट लाभों के लिए पात्रता की गणना करने में मदद करती है।
धारा 57 का उपयोग कहां किया जाता है?
- पैरोल और फर्लो: कुछ जेल नियम सजा का एक हिस्सा पूरा करने के बाद पैरोल की अनुमति देते हैं। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों के लिए, धारा 57 ऐसी गणना के लिए आधार मूल्य प्रदान करती है।
- छूट योजनाएँ: राज्य अक्सर सजा में छूट प्रदान करते हैं। उचित अंश लागू करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग करके सेवा की गई अवधि को मापा जाता है।
- वैधानिक अयोग्यताएं: उदाहरण के लिए, चुनाव कानून दो साल से अधिक की सजा वाले व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करते हैं। जहाँ आवश्यक हो, धारा 57 आजीवन कारावास के तुलनात्मक उपाय को परिभाषित करने में मदद करती है।
बीएनएस, 2023 के तहत स्थिति
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत, जो आईपीसी की जगह लेती है, आईपीसी धारा 57 का सार धारा 6 के तहत बरकरार रखा गया है।
बीएनएस धारा 6 का पाठ:
"दंड की अवधि के अंशों की गणना करने के लिए, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा।"
यह भारत के सुधारित आपराधिक संहिता में प्रावधान की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाता है।
यह अभी भी क्यों मायने रखता है
यद्यपि प्रक्रियात्मक, आईपीसी धारा 57 मायने रखती है के लिए:
- सजा लाभों से संबंधित कानूनों के सुसंगत और निष्पक्ष अनुप्रयोग में सहायता करता है
- यह सुनिश्चित करता है कि आजीवन कारावास जैसी अनिश्चित सजाएं व्यवहार में गणना योग्य हैं
- जेल अधिकारियों या अदालतों द्वारा दुरुपयोग या मनमानी व्याख्या को रोकता है
- कानून के शासन और सजा में एकरूपता के सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है
बीएनएस में इसकी निरंतर उपस्थिति सजा के मामलों में कानूनी स्पष्टता बनाए रखने में इसके महत्व को उजागर करती है।
निष्कर्ष
आईपीसी की धारा 57 कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आजीवन कारावास की सजा के अंशों की गणना करने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदान करती है। यह आजीवन कारावास की परिभाषा को नहीं बदलता है भारतीय न्याय संहिता में इसका स्थान भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में इसकी निरंतर प्रासंगिकता की पुष्टि करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1. आईपीसी धारा 57 क्या है?
यह सजा के अंशों की गणना करते समय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के रूप में माना जाने की अनुमति देता है, जैसे कि पैरोल या छूट के लिए।
प्रश्न 2. क्या इससे आजीवन कारावास की सजा 20 वर्ष हो जाती है?
नहीं, आजीवन कारावास का मतलब अभी भी दोषी को पूरी ज़िंदगी कैद में रहना है। धारा 57 केवल प्रशासनिक गणना में मदद करती है।
प्रश्न 3. धारा 57 कब लागू होती है?
इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कानून या नियम के तहत सजा के एक हिस्से की गणना की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक तिहाई या आधा, विशेष रूप से आजीवन कारावास की सजा वाले मामलों में।
Q4. क्या नई भारतीय न्याय संहिता में धारा 57 शामिल है?
हां, इसे उसी शब्दावली और उद्देश्य के साथ BNS 2023 की धारा 6 के रूप में आगे बढ़ाया गया है।
प्रश्न 5. क्या सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान की व्याख्या की है?
हां, गोडसे के मामले में, न्यायालय ने माना कि आजीवन कारावास अपराधी के पूर्ण प्राकृतिक जीवन के लिए है और धारा 57 केवल सजा-संबंधी गणनाओं में सीमित उपयोग के लिए है।






